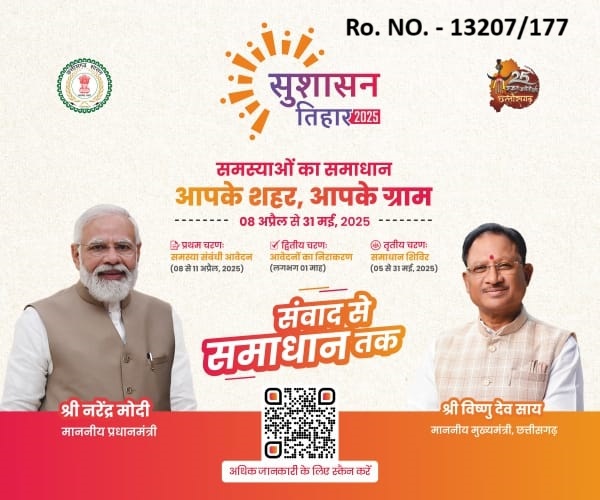Select Date:
कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका: इस टकराव का अंजाम क्या होगा?
Updated on
24-04-2025 03:27 PM

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में विधानसभाअों द्वारा पारित विधेयको को सम्बन्धित राज्यपालों द्वारा अनंत काल तक रोक कर ‘पाॅकेट वीटो’ करने की प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, उससे विधायिका में भारी कसमसाहट है। सत्तापक्ष का मानना है कि यह कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप है। अदालतें कार्यपालिक प्रमुखो जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देशित कैसे कर सकती हैं। दूसरी तरफ न्यायपालिका का मानना है कि यदि कार्यपालिक प्रमुख अपने संवैधानिक दायित्वों की व्याख्या मनमाने और सियासी गुणा भाग के हिसाब से करेंगे तो न्यायपालिका को न्यायदंड अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के इस मामले में सरकार तो सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति भी हैं, ने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट सुपर संसद की तरह काम न करे। हालांकि उपराष्ट्रपति के इस तेवर पर भी विधि विशेषज्ञ दो खेमों में बंट गए हैं, एक इस पर आपवत्ति जता रहा है तो दूसरा इसे ‘साहसिक’ बता रहा है। तो क्या अब संविधान के दो मूलभूत अंग न्यायपालिका और कार्यपालिका ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए सुखकर है? क्या इस सैद्धांतिक द्वंद्व का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा या फिर एक दूसरे की मुश्कें कसने की पूर्वपीठिका तैयार की जा रही है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि वैचारिक द्वंद्व होना अलग बात है और अधिकारों का अतिक्रमण और मर्यादा का सीमांकन की जिद होना दूसरी बात। इस द्वंद्व कार्यपालिका, विधायिका से समर्थन चाहेगी, जो हो भी रहा है। क्योंकि स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका ( जो आज खुद सवालों के घेरे में है) अक्सर कार्यपालिका के कान उमेठती रहती है और कभी कभार विधायिका को भी निर्देशित करती है।
सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल रवि के मामले में स्पष्ट फैसला देते हुए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी की समय सीमा 3 माह तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि इस समयावधि में राज्यपाल विधेयक पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें स्वत: कानून माना जाए। लिहाजा तमिलनाडु में ऐसे 10 विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून बन चुके हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति है। यही नहीं न्यायपालिका ने राज्यपालों के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा भी किसी विधेयक पर मंजूरी की समयावधि तीन माह तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ द्वारा दिए गए इन फैसलों को एक वर्ग न्यायपालिका द्वारा अपनी मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देख रहा है तो समाज का दूसरा वर्ग इसे न्यायपालिका की सक्रियता और निर्भीकता का प्रमाण मान रहा है। इस दूसरे वर्ग का मानना है कि अब लोकतंत्र बचने की आस केवल न्यायपालिका से ही है, क्योंकि बाकी दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाअोंने सत्तातंत्र की दबंगई के आगे घुटने टेक दिए हैं। जबकि सत्तातंत्र जिसमें विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका भी शामिल है, इसे अपने अस्तित्व और वैधता पर न्यायपालिका का स्पष्ट अतिक्रमण मान रही है, जोकि पूरी तरह अस्वीकार्य है। सर्वोच्च अदालत से इस फैसले से सरकार विचलित है। बताया जाता है कि वह जल्द ही इस फैसले पर सुधार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। लेकिन यदि कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखा तो क्या सरकार उसे खारिज करने क्या सरकार नया कानून संसद से पास कराएगी?
यूं यह कानूनी और संवैधानिक बहस का मुद्दा है कि भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों की लक्ष्मण रेखाएं कहां तक हैं? कहां उनका अतिक्रमण होता है और कहां वो शीलभंग के दायरे में हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए? खास कर उस दौर में जहां न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में हो, विधायिका और कार्यपालिका खुद को सर्वेसर्वा मानने लगे।
भारतीय संविधान मूल रूप से तीन पहियों की गाड़ी पर चलता है। ये हैं, विधायिका, जो देश के लिए कानून बनाती है, न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है और उसका पालन करवाने की समीक्षा करती है, और कार्यपालिका जिसका काम कानून पर अमल करवाना है। संविधान में ये तीनो अपने आप में स्वतंत्र लेकिन परस्पर जवाबदेह तथा एक दूसरे को संतुलित करने वाली सत्ताएं हैं। न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं है कि वह विधायिका की जगह ले ले या फिर कार्यपालिका ही किसी कानून की मनमानी व्याख्या करने लगे। कार्यपालिका, जिसके पास वास्तविक सत्ता और अधिकार होते हैं, वह विधायिका और न्यायपालिका दोनो के प्रति जवाबदेह है।
संविधान में राज्यपाल को राज्य का संरक्षक माना गया है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में राज्यपाल दिल्ली सरकार के एजेंट की तरह ही व्यवहार करते हैं और केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के अजेंडे को प्राथमिकता से पूरा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। दिक्कत तब होती है, जब राज्य में विपक्षी पाटी की सरकार होती है। वहां राज्यपालों का व्यवहार राज्य के अभिभावक की तरह कम एक राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ता है। विधानसभा द्वारा पािरत विधेयकों को रोकना और रोकने का कारण भी न बताना संवैधानिक खामियों और राजनीतिक स्वार्थों की वजह भले गलत न लगे, लेकिन राज्यपाल की नीयत पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘अति सक्रियता’ का परिचय देते हुए राज्य और देश के संवैधानिक प्रमुखों की जवाबदेही और समयसीमा तय कर दी। अर्थात यह काम राज्य प्रमुखों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि विधानसभा द्वारा पारित बिल के मामले में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो (पॉकेट वीटो) का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नैतिक रूप से विपक्षी पार्टियों की जीत है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिफरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कुछ बुनियादी संवैधानिक सवाल उठाए हैं, जिनके उत्तर अपेक्षित हैं। उपराष्ट्रपति ने बिलों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा के प्रशिक्षुअो के कार्यक्रम में कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24x7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। आज जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। जबकि सभी को अपनी अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ही सबसे अहम होती है। सभी संस्थाअों को अपनी अपनी सीमाअों में रहकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका द्वारा दूसरे के मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि खुद न्यायपालिका का अपने मामलो में आचरण क्या है? दिल्ली में जस्टिस यशंवत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों? जबकि जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट बरामद हुए थे। ये किसके थे, कहां से आए, कौन और क्यों लाया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं, जिनसे न्यायपालिका के भीतर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को और खाद-पानी मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर जस्टिस की जगह यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ कई जांच एजेंसियां सक्रिय हो जातीं।
जाहिर है कि विधायिका को न्यायपालिका द्वारा उसकी हदें तय करने के फैसले ने विचलित कर िदया है। लेकिन विधायिका की भी कोई जवाबदेही न हो, यह भी उचित नहीं है। इस बात का जवाब अक्सर इस दलील से दिया जाता है िक जनप्रतिनिधियों को हर पांच साल में जनता के बीच जाकर परीक्षा देनी होती है, उसे पास करना होता है। जबकि न्यायपालिका को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोग अदालतों की न्यायदान प्रक्रिया और वास्तविक इंसाफ पर नजर नहीं रखते। सच्चा और निष्पक्ष न्याय हो, समय पर हो और न्याय होता हुआ दिखे भी यही न्यायपालिका की लोकतांत्रिक कसौटी है। लेकिन विधायिका और न्यायपालिका किसी गलती या कर्तव्यपालन में खामी के लिए एक दूसरे को न टोकें, यह भी सही नहीं है। क्योंकि दोनो संविधान और उसकी भावना की रक्षा करने की जिम्मेदारी समान रूप से दोनो की है।
उपराष्ट्रपति ने एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति को निर्देशित करने पर उठाया है। उन्होंने कहा कि अदालत राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में कोई काम करने के लिए कैसे निर्देशित कर सकती है? विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया तय है, लेकिन यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी करना अनिवार्य है, ऐसा उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। यही तर्क केरल के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए दिया था। मगर यहां सवाल केवल समय सीमा भर का नहीं है, बल्कि मंशा का है। यदि कोई बिल राज्यपाल के अधिकार कम करता हो तो भी राज्यपाल को संवैधानिक प्रक्रिया से ही काम करना होगा। क्योंकि उसे मंत्रि परिषद की सलाह से ही काम करना है। अगर राज्यपाल की मंशा ऐसे किसी बिल को लटकाने की है तो राज्य सरकार और विधानसभा क्या करे? संविधान अपनी संस्थाअोंको विवेक से काम करने की आजादी तो देता है, लेकिन मनमर्जी और राजनीतिक दुराग्रह से काम करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्यपालों का व्यवहार आज ही देखने में आ रहा है। पहले भी कुछ राज्यपालो का आचरण दिल्ली के सत्ताधीशों के सियासी हितों साधने से प्रेरित रहा है। इनके आचरण से राज्यपाल संस्था की गरिमा को बट्टा ही लगा।
अजय बोकिल , संपादक
अन्य महत्वपुर्ण खबरें

कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका: इस टकराव का अंजाम क्या होगा?
24 April 2025
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में विधानसभाअों द्वारा पारित विधेयको को सम्बन्धित राज्यपालों द्वारा अनंत काल तक रोक कर ‘पाॅकेट वीटो’ करने की प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय…

छत्तीसगढ़ बन रहा निवेश का नया हब
17 April 2025
रायपुर I छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 218 नई…
14 अप्रैल जयंती पर विशेष : जो समाज पिछड़ा हुआ है उनका नेता अगर सो जाएगा तो वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा : डॉ. अंबेडकर
14 April 2025
भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग याद आता है जब एक बार विदेशी पत्रकारों का प्रतिनिधि मंडल भारत भ्रमण पर आया। यह प्रतिनिधि…

विपक्ष का लक्ष्य परिवार का विकास और संघर्ष मोड में कांग्रेस
13 April 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों यानी इंडिया ब्लाक पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष का एकमेव लक्ष्य परिवार का साथ और परिवार का विकास है। मध्यप्रदेश के…
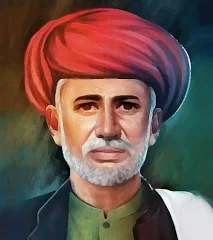
सामाजिक समरसता के स्तंभ आधार: महात्मा ज्योतिबा फुले
11 April 2025
महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ज्योतिबा फुले बचपन से ही सामाजिक समदर्शी तथा होनहार मेधावी छात्र थे, आर्थिक कठिनाइयों के कारण …

‘हिंदू ग्राम’ से ‘हिंदू राष्ट्र’ तक की उड़ान में गुंथी सवालों की डोर - अजय बोकिल
10 April 2025
मप्र के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम स्थित बागेश्वर धाम के स्वयंभू पीठाधीश पं.धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने इलाके में ‘पहला हिंदू ग्राम’ बसाने का ऐलान कर नई बहस को…

देनदारियां चुकाने का दावा करते डॉ. मोहन यादव
06 April 2025
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया है कि बीते वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार ने आठ साल पुरानी देनदारियां चुकाई हैं। उनका कहना है कि यह सब…
.jpg)
भाजपा का समर्थ भारत निर्माण में अतुलनीय योगदान
06 April 2025
विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने स्थापना के 46 वे वर्ष में प्रवेश किया है।भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी,लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी,कुशा भाऊ ठाकरे, राजमाता विजयाराजे…

मनोज कुमार की फिल्मी देशभक्ति ने तैयार की राष्ट्रवादी सत्ता की भावभूमि
05 April 2025
हिंदी फिल्मों में गुजरे जमाने के एक खूबसूरत, खयालों में खोए से और देशभक्ति को अपनी पिक्चरों की केन्द्रीय थीम बनाकर देश को एक अलग तरह का संदेश देने वाले…